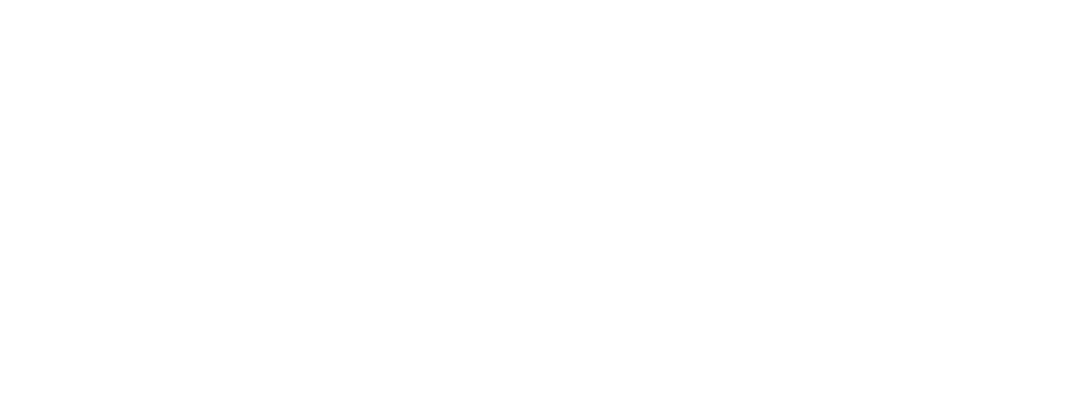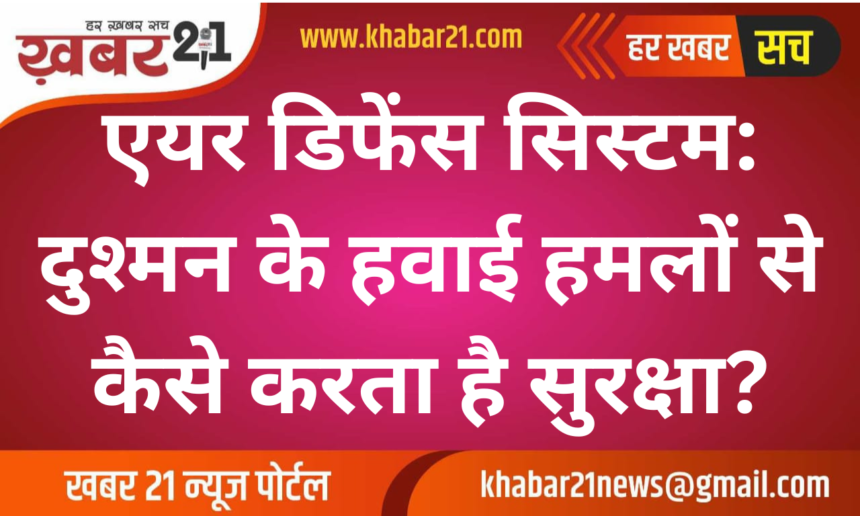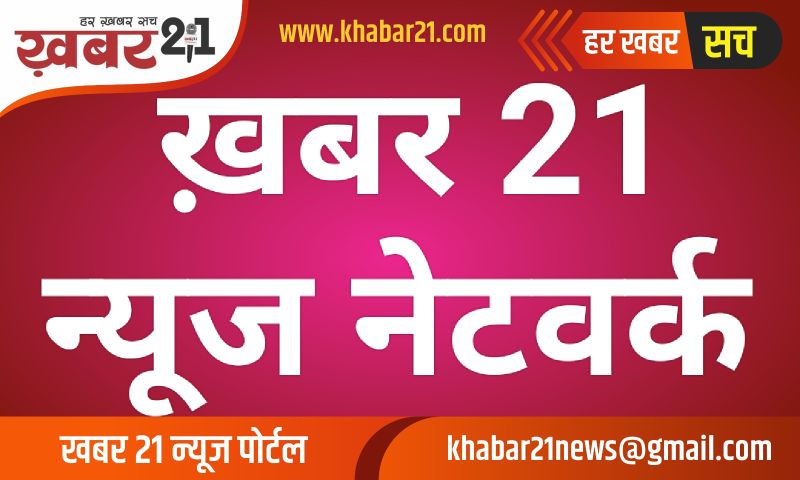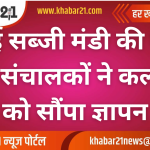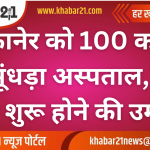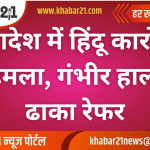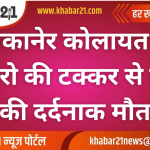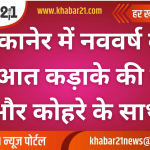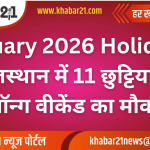भारत का एयर डिफेंस सिस्टम: दुश्मन के हवाई हमलों से कैसे करता है सुरक्षा?
आधुनिक युद्धों में आकाशीय प्रभुत्व हासिल करना निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी कड़ी में एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति का एक अहम स्तंभ बन चुका है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके जवाब में पाकिस्तान ने बुधवार रात भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारत के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी प्रयासों को विफल कर दिया।
गुरुवार सुबह भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई स्थानों पर एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। भारतीय सेना द्वारा जारी बयान में कहा गया, “विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर लाहौर में स्थित एक एयर डिफेंस यूनिट को निष्क्रिय किया गया है। हमारी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की कार्रवाई की तीव्रता और क्षेत्र के अनुसार संतुलित रही।”
एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और कैसे करता है काम?
एयर डिफेंस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के हवाई खतरों—जैसे फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइलों—को समय रहते पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करना होता है। यह सिस्टम आम तौर पर रडार, कमांड सेंटर, डिफेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट, एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीकों का समन्वय होता है।
- Advertisement -
1. डिटेक्शन (पता लगाना)
एयर डिफेंस का पहला कदम है खतरे की जल्द से जल्द पहचान करना। यह रडार के जरिए होता है, जो उच्च आवृत्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वातावरण में भेजता है। ये तरंगें किसी वस्तु (जैसे विमान या मिसाइल) से टकराकर वापस लौटती हैं और रिसीवर उन्हें पकड़कर उनकी दूरी, गति और प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मामलों में सैटेलाइट डिटेक्शन की भी भूमिका होती है।
2. ट्रैकिंग (नज़र बनाए रखना)
खतरे को केवल पहचानना पर्याप्त नहीं है, उस पर लगातार निगरानी बनाए रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए इंफ्रारेड सेंसर, लेज़र रेंजफाइंडर और अन्य उन्नत तकनीकों का सहारा लिया जाता है। कई बार एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ कई दिशाओं से आने वाले खतरों से निपटना पड़ता है, जिससे गलती की संभावना बढ़ जाती है। सटीक ट्रैकिंग नागरिक विमानों को नुकसान से बचाने में भी सहायक होती है।
3. इंटरसेप्शन (निष्क्रिय करना)
आखिरी चरण होता है खतरे को समाप्त करना। दुश्मन के हथियार की प्रकृति (मिसाइल, ड्रोन या विमान), उसकी गति, ऊंचाई और दिशा के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन-सा प्रतिरक्षा उपाय अपनाया जाए। भारत के पास मौजूद S-400 ट्रायंफ जैसे सिस्टम इन खतरों को 400 किलोमीटर दूर से ही निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं।
भारत का रक्षा कवच क्यों है खास?
भारत के पास रूसी S-400 ट्रायंफ सिस्टम, स्वदेशी आकाश मिसाइल, बाराक़-8, SPYDER और इजरायली आयरन डोम जैसी कई अत्याधुनिक तकनीकें हैं। यह संयोजन भारत की वायु सीमाओं को दुनिया के सबसे मजबूत सुरक्षा घेरों में से एक बनाता है।
हालिया घटनाओं में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम की सटीकता और ताकत ने यह साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ आक्रमण का जवाब देने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के इरादों को समय रहते नाकाम करने में भी निपुण है।